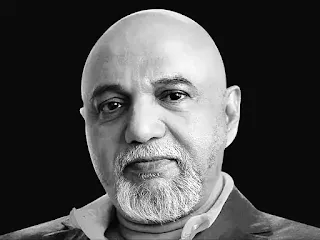हिंदी पत्रकारिता के 200 साल
-प्रो.संजय द्विवेदी
हिंदी पत्रकारिता के 200 साल की यात्रा का उत्सव
मनाते हुए हमें बहुत से सवाल परेशान कर रहे हैं जिनमें सबसे खास है ‘संपादक का विस्थापन’। बड़े होते मीडिया संस्थान जो
स्वयं में एक शक्ति में बदल चुके हैं, वहां संपादक की सत्ता और महत्ता दोनों कम
हुई है। अखबारों से खबरें भी नदारद हैं और विचार की जगह भी सिकुड़ रही है। बहुत
गहरे सौंदर्यबोध और तकनीकी दक्षता से भरी प्रस्तुति के बाद भी अखबार खुद को संवाद
के लायक नहीं बना पा रहे हैं। यह ऐसा कठिन समय है जिसमें रंगीनियां तो हैं पर
गहराई नहीं। हर तथ्य और कथ्य का बाजार पहले ढूंढा जा रहा है, लिखा बाद में जा रहा
है।
नए
समय में पत्रकारिता को सिर्फ कौशल या तकनीक के सहारे चलाने की कोशिशें हो रही हैं।
जबकि पत्रकारिता सिर्फ कौशल नहीं बहुत गहरी संवेदना के साथ चलने वाली विधा है।
जहां शब्द हैं, विचार हैं और उसका समाज पर पड़ने वाला प्रभाव है। ऐसे में सवाल यह
उठता है कि क्या पत्रकारिता के पारंपरिक मूल्य और सिद्धांत अप्रासंगिक हो गए हैं
या नए जमाने में ऐसा सोचना ठीक नहीं है। डिजीटल मीडिया की मोबाइल जनित व्यस्तता ने
पढ़ने, गुनने और संवाद का सारा समय खा-पचा लिया है। जो मोबाइल पर आ रहा है,वही
हमें उपलब्ध है। हम इसी से बन रहे हैं, इसी को सुन और गुन रहे हैं। ऐसे खतरनाक समय
में जब अखबार पढ़े नहीं, पलटे जाने की भी प्रतीक्षा में हैं। दूसरी ओर वाट्सअप में
अखबारों के पीडीएफ तैर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो पीडीएफ पर ही छपते हैं। अखबारों को
हाथ में लेकर पढ़ना और ई-पेपर की तरह पढ़ना दोनों के अलग अनुभव हैं। नई पीढ़ी
मोबाइल सहज है। उसने मीडिया घरानों के एप मोबाइल पर ले रखे हैं। वे अपने काम की
खबरें देखते हैं। ‘न्यूज यू कैन यूज’ का नारा अब सार्थक हुआ है। खबरें भी पाठकों को चुन रही हैं और पाठक भी
खबरों को चुन रहे हैं। यह कहना कठिन है कि अखबारों की जिंदगी कितनी लंबी है। 2008
में ‘प्रिंट इज डेट किताब’ लिखकर जे. गोमेज इस अवधारणा को बता चुके हैं।
सवाल
यह नहीं है कि अखबार बचेंगे या नहीं मुद्दा यह है कि पत्रकारिता बचेगी या नहीं।
उसकी संवेदना, उसका कहन, उसकी जनपक्षधरता बचेगी या नहीं। संपादक की सत्ता
पत्रकारिता की इन्हीं भावनाओं की संरक्षक थी। संपादक अखबार की संवेदना, भाषा, उसके
वैचारिक नेतृत्व,समाजबोध का संरक्षण करता था। उसकी विदाई के साथ कई मूल्य भी विदा
हो जाएंगें। गुमनाम संपादकों को अब लोग समाज में नहीं जानते हैं। खासकर हिंदी
इलाकों में अब पहचान विहीन और ‘ब्रांड’ वादी अखबार निकाले जा रहे हैं। अब संपादक के होने न होने से फर्क नहीं पड़ता।
उसके लिखने न लिखने से भी फर्क नहीं पड़ता। न लिखे तो अच्छा ही है। पहचानविहीन
चेहरों की तलाश है, जो अखबार के ब्रांड को चमका सकें। संपादक की यह विदाई अब उस
तरह से याद भी नहीं की जाती। पाठकों ने ‘नए अखबार’ के साथ अनुकूलन कर लिया है। ‘नया अखबार’ पहले पन्ने पर भी किसी भी प्रोडक्ट का एड छाप सकता है, संपादकीय पन्ने को
आधा कर विचार को हाशिए लगा सकता है। खबरों के नाम पर एजेंडा चला सकता है। ‘सत्य’ के बजाए यह ‘नरेटिव’ के साथ खड़ा है। यहां सत्य रचे और तथ्य गढ़े जा सकते हैं। उसे बीते हुए
समय से मोह नहीं है वह नए जमाने का ‘नया अखबार’ है। वह विचार और समाचार नहीं कंटेट गढ़ रहा है। उसे बाजार में छा जाने की
ललक है। उसके टारगेट पर खाये-अघाए पाठक हैं जो उपभोक्ता में तब्दील होने पर आमादा
हैं। उसके कंटेंट में लाइफ स्टाइल की प्रमुखता है। वह जिंदगी को जीना और मौज सिखाने
में जुटा है। इसलिए उसका जोर फीचर पर है, अखबार को मैग्जीन बनाने पर है। अखबार
बहुत पहले ‘रंगीन’ हो चुका है, उसका
सारा ध्यान अब अपने सौंदर्यबोध पर है। वह ‘प्रजेंटेबल’ बनना चाहता है। अपनी समूची प्रस्तुति में ज्यादा रोचक और ज्यादा जवान।
उसे लगता है कि उसे सिर्फ युवा ही पढ़ते हैं और वह यह भी मानकर चलता है कि युवा को
गंभीर चीजें रास नहीं आतीं।
यह ‘नया अखबार’ अब संपादक की निगरानी से मुक्त है।
मूल्यों से मुक्त। संवेदनाओं से मुक्त। भाषा के बंधनों से मुक्त। यह भाषा सिखाने
नहीं बिगाड़ने का माध्यम बन रहा है। मिश्रित भाषा बोलता हुआ। संपादक की विदा के
बहुत से दर्द हैं जो दर्ज नहीं है। नए अखबार ने मान लिया है कि उसे नए पाठक चुनने
हैं। बनाना है उन्हें नागरिक नहीं, उपभोक्ता। ऐसे कठिन समय में अब सक्रिय पाठकों
का इंतजार है। जो इस बदलते अखबार की गिरावट को रोक सकें। जो उसे बता सकें कि उसे
दृश्य माध्यमों से होड़ नहीं करनी है। उसे शब्दों के साथ होना है। विचार के साथ
होना है।
हिंदी
के संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर ने कहा था, ‘‘पत्र निकालकर सफलतापूर्वक चलाना बड़े-बड़े धनियों अथवा सुसंगठित कंपनियों
के लिए ही संभव होगा। पत्र सर्वांग सुंदर होंगे। आकार बड़े होंगे, छपाई अच्छी होगी, मनोहर, मनोरंजक
और ज्ञानवर्द्धक चित्रों से सुसज्जित होंगे, लेखों में
विविधता होगी, कल्पकता होगी, गंभीर
गवेषणा की झलक होगी, ग्राहकों की संख्या लाखों में गिनी
जाएगी। यह सब कुछ होगा पर पत्र प्राणहीन होंगे। पत्रों की नीति देशभक्त, धर्मभक्त अथवा मानवता के उपासक महाप्राण संपादकों की नीति न होगी- इन
गुणों से संपन्न लेखक विकृत मस्तिष्क समझे जाएंगे, संपादक की
कुर्सी तक उनकी पहुंच भी न होगी। वेतनभोगी संपादक मालिक का काम करेंगे और बड़ी
खूबी के साथ करेंगे। वे हम लोगों से अच्छे होंगे। पर आज भी हमें जो स्वतंत्रता
प्राप्त है वह उन्हें न होगी। वस्तुतः पत्रों के जीवन में यही समय बहुमूल्य है।”
श्री
पराड़कर की यह भविष्यवाणी आज सच होती हुई दिखती है। समानांतर प्रयासों से कुछ लोग
विचार की अलख जगाए हुए हैं। लेकिन जरूरी है कि हम अपने पाठकों के सक्रिय सहभाग से
मूल्य आधारित पत्रकारिता के लिए आगे आएं। तभी उसकी सार्थकता है।