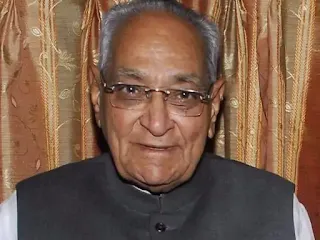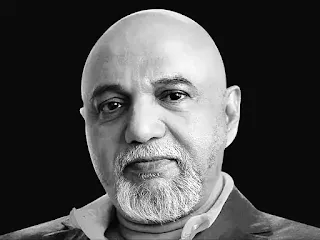- प्रो. (डा.) संजय
द्विवेदी
इन दिनों देश में लोकतंत्र का महापर्व
चल रहा है। राजनीति का आकर्षण प्रबल है। सिने कलाकार,
साहित्यकार, वकील, न्यायाधीश,
खिलाड़ी, गायक, उद्योगपति
सब क्षेत्रों के लोग राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं। ऐसा ही हाल पत्रकारिता के
सितारों का भी है। मीडिया और पत्रकारिता के अनेक चमकीले नाम राजनीति के मैदान में
उतरे और सफल हुए।
आजादी के आंदोलन में तो
मीडिया को एक तंत्र की तरह इस्तेमाल करने के लिए प्रायः सभी वरिष्ठ राजनेता
पत्रकारिता से जुड़े और उजली परंपराएं खड़ी कीं। बालगंगाधर तिलक, महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चन्द्र बोस, महामना पं.मदनमोहन
मालवीय, पंडित नेहरू सभी पत्रकार थे। आजादी के बाद बदलते दौर
में पत्रकारिता और राजनीति की राहें अलग-अलग हो गईं, लेकिन
सत्ता का आकर्षण बढ़ गया। जनपक्ष, राष्ट्र सेवा की
पत्रकारिता अब आजाद भारत में राष्ट्र निर्माण का भाव भरने में लगी थी। सेवा
राजनीति के माध्यम से भी की जा सकती है, यह भाव भी प्रबल
हुआ।
मूल्यों पर ‘अटल’ रहने वाले ‘वाजपेयी’-
राजनीतिक
दलों से संबंधित समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के
अलावा मुख्यधारा की पत्रकारिता से भी लोग राजनीति में आए, जिसमें
सबसे खास नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी का है।वे 'वीर अर्जुन' जैसे दैनिक अखबार के संपादक थे। इसके साथ ही वे 'स्वदेश',
'पांचजन्य' और 'राष्ट्रधर्म'
के भी संपादक भी थे। वे जहां संसदीय राजनीति के लंबे अनुभव के साथ
प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी रहे, तो वहीं भाजपा के
संस्थापक अध्यक्ष भी थे। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी 'हिंदुस्तान समाचार' और 'ऑर्गनाइजर'
से संबद्ध थे, फिर राजनीति में आए।
कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष
रहे पं.कमलापति त्रिपाठी जाने-माने पत्रकार थे। ‘आज’(वाराणसी) के संपादक के रूप में उन्होंने ख्याति अर्जित की। बाद में वे
लोकसभा के सदस्य चुने गए और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। मध्यप्रदेश के पूर्व
मुख्यमंत्री पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र ने दैनिक 'लोकमत',
साप्ताहिक 'सारथी' और 'श्री शारदा' के संपादक के रूप में ख्याति अर्जित
की।तत्कालीन विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शंभूनाथ शुक्ल बाद में बने मध्यप्रदेश
में मंत्री और सांसद रहे। 'विशाल भारत' के संपादक रहे बनारसी दास चतुर्वेदी दो बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित
हुए। गणेश शंकर विद्यार्थी के शिष्य बालकृष्ण शर्मा नवीन 'प्रताप'
के संपादक थे और कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचे। महाराष्ट्र का दर्डा
परिवार राजनीति में अग्रणी स्थान रखता है । 'लोकमत' समाचार के संस्थापक जवाहरलाल दर्डा, राजेन्द्र दर्डा
और विजय दर्डा सांसद, विधायक और मंत्री रहे। 'विजया कर्नाटक' और 'कन्नड़
प्रभा' अखबार से जुड़े रहे प्रताप सिम्हा भाजपा से दो बार
लोकसभा पहुंचे। उनका नाम चर्चा में तब आया, जब उनके द्वारा
अनुमोदित विजिटर पास से दो युवकों ने नई संसद में पहुंच कर हंगामा किया। अंग्रेजी
के नामवर पत्रकार खुशवंत सिंह राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य के रूप राष्ट्रपति
द्वारा नामित किए गए। सपा ने दैनिक जागरण के मालिकों में एक महेंद्र मोहन गुप्त को
उप्र से राज्यसभा भेजा।
मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ तक सितारों की जगमगाहट-
मूलतः पत्रकारिता से
सार्वजनिक जीवन में आए मोतीलाल वोरा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। मध्यप्रदेश के
पूर्व मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल ने रायपुर से 'दैनिक
महाकौशल' अखबार निकाला। भाजपा के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
दोनों राज्यों के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद बने लखीराम अग्रवाल ने बिलासपुर से 'लोकस्वर' अखबार निकाला। बिलासपुर के पत्रकार बीआर
यादव मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री और चार बार विधायक चुने गए। स्वतंत्रता संग्राम
सेनानी ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी नवभारत, नागपुर के संपादक थे और बाद में सांसद बने।
नवीन दुनिया, जबलपुर के संपादक मुंदर शर्मा विधायक और सांसद दोनों पदों पर चुने
गए। जबलपुर से प्रहरी (साप्ताहिक) के संपादक रहे उसी शहर से मेयर और 2 बार
राज्यसभा के सदस्य थे।
बिलासपुर
के रहने वाले कवि, पत्रकार श्रीकांत
वर्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सदस्य बने। वे 'दिनमान' के संपादक मंडल में रहने के बाद राजनीति में
आए थे । छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रहने वाले चंदूलाल चंद्राकर दैनिक 'हिन्दुस्तान' के संपादक बने। बाद में कांग्रेस ने
उन्हें राज्यसभा में भेजा। चंद्राकर, राजीव गांधी की सरकार में मंत्री भी बने
किंतु एक विवाद में नाम आने पर उनका इस्तीफा ले लिया गया। नवभारत से जुड़े रहे
राजनांदगांव के पत्रकार लीलाराम भोजवानी छत्तीसगढ़ सरकार में श्रम मंत्री थे। 'देशबन्धु' में पत्रकारिता का पाठ पढ़ने वाले
चंद्रशेखर साहू छत्तीसगढ़ से सांसद, मंत्री और विधायक बने।
मध्यप्रदेश में सीहोर के पत्रकार शंकर लाल साहू विधायक थे। दमोह के आनंद
श्रीवास्तव भी पत्रकार थे, बाद में विधायक बने। त्रिभुवन यादव पिपरिया से विधायक बने।
कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे और दो बार विधायक चुने गए विष्णु राजोरिया मूलतः
पत्रकार ही हैं, बाद में उन्होंने 'शिखर
वार्ता' पत्रिका भी निकाली। मप्र में ही केएन प्रधान सांसद,
विधायक और मंत्री भी थे। नागपुर के अंग्रेजी अखबार 'हितवाद' के प्रकाशन करने वाले बनवारी लाल पुरोहित
कांग्रेस और भाजपा दोनों से लोकसभा पहुंचे। संप्रति वे पंजाब के राज्यपाल हैं।
भाजपा हो या कांग्रेस,
सबने दिये मौके-

कांग्रेस ने अंग्रेजी के दिग्गज पत्रकार कुलदीप
नैयर, एचके दुआ (हिंदुस्तान टाइम्स), हिंदी के राजीव शुक्ला,
प्रफुल्ल कुमार माहेश्वरी, मराठी के कुमार
केतकर आदि को राज्यसभा से नवाजा। राजीव शुक्ला मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री
भी रहे। शिवसेना से अंग्रेजी के पत्रकार और फिल्ममेकर प्रतीश नंदी राज्यसभा
पहुंचे। ‘पांचवा स्तंभ’ नामक मासिक
पत्रिका निकालने वाली मृदुला सिन्हा गोवा की राज्यपाल बनीं। ‘चौथी दुनिया’ के संपादक संतोष भारतीय भी जनता दल से फरूखाबाद से लोकसभा पहुंचे। वरिष्ठ
पत्रकार संजय निरुपम भी लोकसभा पहुंचे, वे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 'सामना' के संपादक संजय राऊत अपने धारदार बयानों के
लिए लोकप्रिय हैं, वे भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना से राज्यसभा
सदस्य हैं। जनता दल (यू) ने प्रभात खबर के संपादक रहे हरिवंश नारायण सिंह को दो
बार राज्यसभा भेजा, वे इन दिनों राज्यसभा के उपसभापति भी
हैं। 'ऑर्गनाइजर' के संपादक रहे श्री
के.आर.मलकानी बाद में राज्यसभा पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने अरूण शौरी, चंदन
मित्रा, स्वप्नदास गुप्ता, दीनानाथ मिश्र, बलबीर पुंज, राजनाथ सिंह सूर्य, नरेन्द्र मोहन, प्रभात झा, तरुण
विजय को राज्यसभा भेजा। शौरी वाजपेयी
सरकार में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री थे। उनके पास विनिवेश मंत्री का
कार्यभार भी था। इनमें चंदन मित्रा बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो
गए, जबकि पुंज और झा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी मनोनीत
हुए। प्रभात झा मध्यप्रदेश भाजपा के चर्चित अध्यक्ष भी थे। भाजपा और कांग्रेस
दोनों दलों में रह चुके वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर किशनगंज से कांग्रेस के टिकट पर
लोकसभा पहुंचे। बाद में भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा और विदेश राज्यमंत्री
बनाया। मोदी सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के
रूप में कार्य कर चुके रमेश पोखरियाल निशंक का पत्रकारिता से गहरा नाता रहा है। वे
दैनिक जागरण से जुड़े थे, साथ ही स्वयं का ‘सीमांत वार्ता’ नाम का अखबार भी प्रकाशित किया।हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश
कौशिक भी मूलतः पत्रकार हैं। वह दिल्ली और शिमला में पत्रकारिता की लंबी पारी के
बाद राजनीति में आए। हरियाणा के अंबाला लोकसभा क्षेत्र से 2014 में भाजपा सांसद चुने गए अश्विनी कुमार अब इस दुनिया में नहीं हैं,
लेकिन 'पंजाब केसरी' के
माध्यम से की गई उनकी धारदार पत्रकारिता लोगों के जेहन में है। 'इकोनॉमिक टाइम्स' में रहे देवेश कुमार बिहार में
भाजपा से विधान परिषद में है और प्रदेश महामंत्री भी हैं। हरियाणा सरकार में वित्त
मंत्री बने कैप्टन अभिमन्यु भी दैनिक 'हरिभूमि' के संपादक, प्रकाशक थे।
क्षेत्रीय दलों ने भी दिए अवसर-
तृणमूल कांग्रेस ने हाल में ही अंग्रेजी की
पत्रकार सागरिका घोष को राज्यसभा भेजा है। इसके पूर्व उर्दू पत्रकारिता से जुड़े रहे नदीमुल हक भी तृणमूल
से राज्यसभा पहुंचे। हिंदी अखबार 'सन्मार्ग'
के मालिक विवेक गुप्ता तृणमूल से सांसद भी रहे, अब विधानसभा में हैं। कुणाल घोष भी इसी दल से राज्यसभा पहुंचे। उर्दू के पत्रकार शाहिद सिद्दीकी (उर्दू नई
दुनिया) सपा से, तो मीम अफजल (अखबार-ए-नौ) कांग्रेस से
राज्यसभा पहुंचे। शाहिद सपा, कांग्रेस, आरएलडी की परिक्रमा करके फिर सपा में हैं।
आंध्र प्रदेश से छपने वाले तेलुगु अखबार 'वार्ता' के संपादक गिरीश सांघी कांग्रेस से राज्यसभा हो आए। पत्रकारिता से जुड़े
रहे तेलंगाना के के. केशवराव कांग्रेस और टीआरएस दोनों दलों से राज्यसभा जा चुके
हैं। कोलकाता के पत्रकार अहमद सईद मलीहाबादी भी राज्यसभा पहुंचे। जनता दल (यूनाइटेड)
से एजाज अली भी राज्यसभा (2008 से 2010) में रहे। टीवी पत्रकार मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं में
हैं और दिल्ली सरकार में उपमुख्यमंत्री बने। संप्रति वे शराब घोटाले के आरोप में
तिहाड़ जेल में हैं।
कुछ पत्रकार लोकसभा चुनाव लड़कर भी संसद नहीं
पहुंच पाए। जैसे वरिष्ठ पत्रकार उदयन शर्मा, सुप्रिया श्रीनेत (कांग्रेस), साजिया
इल्मी, आशीष खेतान, आशुतोष (आप), और सीमा मुस्तफा जनता दल के टिकट पर लोकसभा नहीं
पहुंच सके। साजिया अब बीजेपी में आ चुकी हैं।
कुछ ने नेपथ्य में तलाशी संभावनाएं-
अनेक
दिग्गज पत्रकार चुनावी समर में उतरने के बजाए नेपथ्य में ताकतवर रहे और अपने समय
की राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी
के साथ मीडिया सलाहकार एच.वाई. शारदा प्रसाद ने ‘इंडियन एक्सप्रेस’ से अपना कैरियर प्रारंभ किया था।
बाद में वे इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मासकम्युनिकेशन और नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट की
स्थापना में सहयोगी थे। उन्हें पद्मविभूषण से भी अलंकृत किया गया। ‘इंडिया टुडे’ के पत्रकार सुमन दुबे भी राजीव गांधी
के मीडिया सलाहकार थे। अब वे राजीव गांधी फाउंडेशन का काम देख रहे हैं। इसके अलावा
प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ रहे अशोक टंडन, सुधीन्द्र कुलकर्णी,हरीश खरे,
पंकज पचौरी, संजय बारू के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें टंडन और कुलकर्णी अटल जी के
साथ और खरे,पचौरी, तथा बारू मनमोहन सिंह के साथ थे। बारू बाद में अपनी किताब ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ लिखकर विवादों में भी
आए।
राजनीति के मंच पर ऐसे अनेक सितारे चमके और
अपनी जगह बनाई। तमाम ऐसे भी थे, जो पार्टी के प्रवक्ता या
बौद्धिक कामों से संबद्ध थे। तमाम अज्ञात ही रह गये। राजनीति वैसे भी कठिन खेल है,
संभावनाओं से भरा भी। किंतु सबको इसका फल मिले यह जरूरी नहीं।
बावजूद इसके इसका आकर्षण कम नहीं हो रहा। वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी कहते थे,
"पत्रकार की पोलिटिकल लाइन तो ठीक है, पर
पार्टी लाइन नहीं होनी चाहिए।" किंतु यह
लक्ष्मण रेखा भी टूट रही है। क्यों, इस पर सोचिए जरूर।